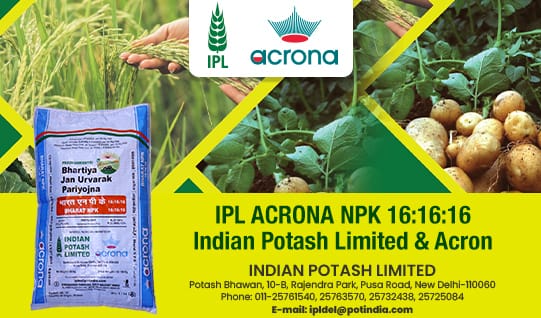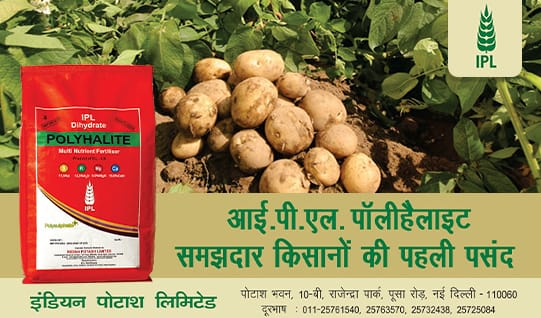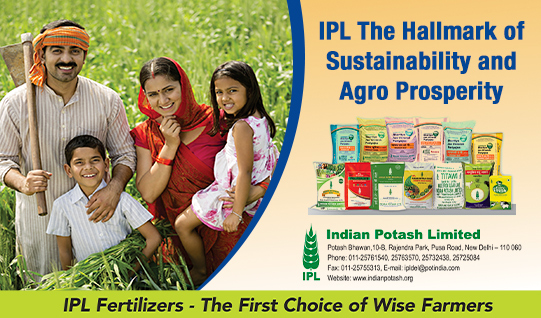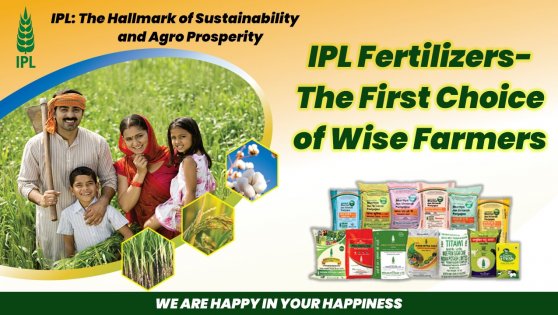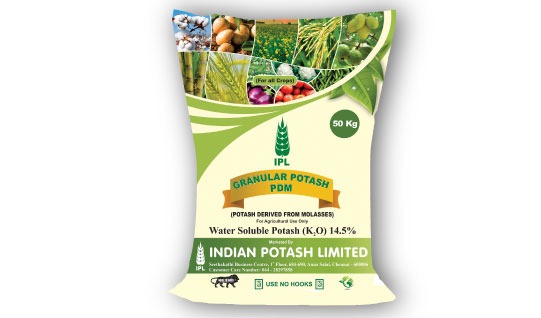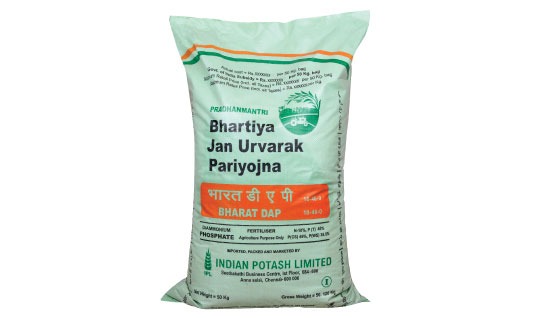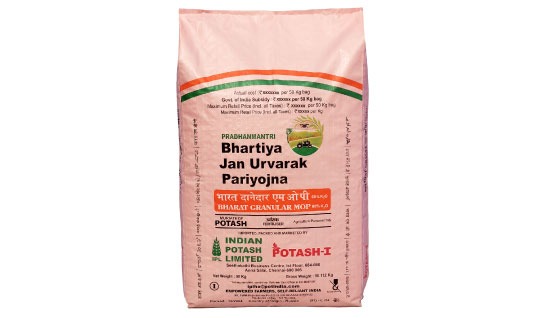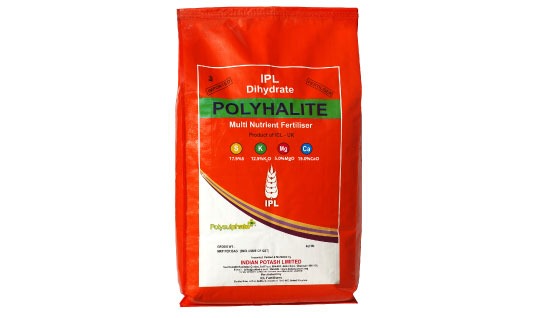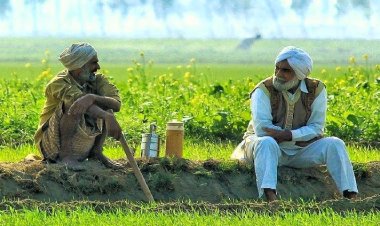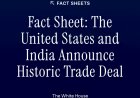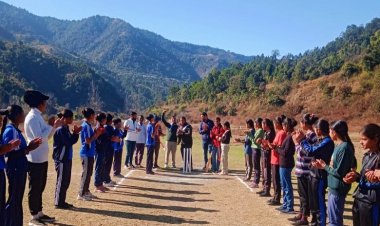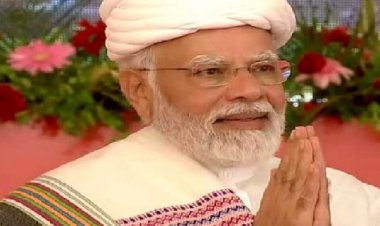प्लांट वैरायटी एक्ट के संशोधन में कृषक अधिकारों की सुरक्षा जरूरी
भारत ने दो दशक बाद प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स’ राइट्स एक्ट में संशोधन शुरू किया है, ताकि क्रियान्वयन की खामियों को दूर किया जा सके और कानूनी प्रावधानों को स्पष्ट किया जा सके। 12 सदस्यीय समिति किसानों और बीज उद्योग सहित हितधारकों की प्रतिक्रिया की समीक्षा कर रही है। आधे से अधिक वैरायटी सर्टिफिकेट किसानों की किस्मों को मिलने के बावजूद संस्थागत समर्थन की कमी, उद्योग की तरफ से अधिक आईपी-हितैषी सुधारों का दबाव और किसानों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।

भारत ने कृषि और बागवानी फसलों की किस्मों, पादप प्रजनन (plant breeding) और किसानों के अधिकारों से संबंधित बौद्धिक संपदा (आईपी) कानून - पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीपीवी एंड एफआर अधिनियम) - में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह अधिनियम मूल रूप से 30 अक्टूबर 2001 को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के प्रावधानों के अनुपालन में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। यह कानून दो चरणों में लागू हुआ। पहले चरण की धाराएं 11 नवंबर 2005 से और दूसरे चरण की शेष धाराएं 19 अक्टूबर 2006 से प्रभावी हुईं।
प्रस्तावित संशोधनों के लिए मुख्य तर्क यह दिया गया कि कानून के लागू होने के बीस वर्ष बाद इसके क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों को दूर करने की आवश्यकता है। अधिकारी कुछ कानूनी प्रावधानों में स्पष्टता की आवश्यकता भी बताते हैं। इस कानून में अब तक केवल एक बार, वर्ष 2021 में संशोधन किया गया था।
पीपीवी एंड एफआर प्राधिकरण का मुख्यालय 2005 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया। तब से इसने गुवाहाटी, पालमपुर, पुणे, रांची और शिवमोगा में पांच क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं। यह प्राधिकरण नई और मौजूदा पौध किस्मों की 206 श्रेणियों पर बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान करता है। पंजीकरण के लिए आवेदन स्वीकृत होने पर पौध किस्म प्रमाणपत्र (पीवीसी) जारी किया जाता है। पीपीवी एंड एफआर अधिनियम के तहत ‘पंजीकरण’ में प्लांट ब्रीडर को 15 वर्षों (फसलों के लिए) और 18 वर्षों (पेड़/लता के लिए) की अवधि के लिए उस किस्म का उत्पादन, बिक्री, विपणन, वितरण, आयात या निर्यात करने के विशिष्ट अधिकार प्रदान करता है।
प्राधिकरण ने ‘अधिनियम और नियमों की समीक्षा कर संशोधन के सुझाव देने’ के लिए एक समिति गठित की है। यह समिति 3 दिसंबर 2024 को आयोजित प्राधिकरण की 39वीं बैठक में अनुमोदित की गई। बारह सदस्यीय समिति की अध्यक्षता कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई) के सेवानिवृत्त सचिव एवं आईसीएआर के पूर्व महानिदेशक डॉ. आर.एस. परोदा कर रहे हैं। इसमें बीज उद्योग सहित विविध हितधारक समूहों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
हितधारकों के साथ परामर्श अक्टूबर 2025 के अंत तक हाइब्रिड मोड में आयोजित किए गए। इनमें बीज उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र एवं किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली स्थित प्लांट अथॉरिटी भवन में भाग लिया। इन परामर्शों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर समिति कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को सुझाव देगी।
जब यह कानून पहली बार पारित किया गया था, तब इसे कृषि में आईपी के डब्ल्यूटीओ मानदंडों के अनुरूप ढलती दुनिया के बीच भारत का अनूठा उत्तर बताया गया था। यहां किसानों के नवाचार को न तो मान्यता मिलती थी और न ही कोई प्रतिफल। भारत के इस आईपी कानून की विशिष्टता यह है कि यह किसानों को भी ब्रीडर के रूप में मान्यता देता है और उन्हें अपनी किस्मों पर आईपी प्राप्त करने का विकल्प प्रदान करता है। प्राधिकरण के प्रयास अधिक किसानों को पंजीकरण के लिए प्रेरित करने और उनकी किस्मों को आईपी व्यवस्था में शामिल करने की ओर रहे हैं। हालांकि अनेक किसान पौधों पर विशिष्ट संपत्ति अधिकार की अवधारणा के विरोध के चलते ऐसे आईपी पंजीकरण से दूर भी रहे हैं। कुछ इसके बजाय गैर-आईपी आधारित संस्थागत समर्थन चाहते हैं, जिसमें पीवीसी के लिए पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं होता। कुछ का तर्क है कि कॉमन जैव-सांस्कृतिक विरासत के रूप में उपयोग और संरक्षित किस्मों को किसी एक किसान के इनोवेशन के रूप में आईपी का अधिकार देना उचित नहीं है।
पीपीवी एंड एफआर प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 31 अक्टूबर 2025 तक कुल 10,018 पीवीसी जारी किए गए हैं। इनमें से 5,038 किसान किस्मों (एफवी) को दिए गए। प्राधिकरण इस तथ्य को रेखांकित करता है कि अब तक जारी कुल आईपी पंजीकरणों में किसानों की किस्मों पर आईपी की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है।
फिर भी दो गुणात्मक तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला, किसान द्वारा तैयार किस्में ‘विद्यमान’ (या मौजूदा) श्रेणी में पंजीकृत हैं, ‘नई’ श्रेणी में नहीं। यदि किसान ब्रीडर द्वारा खेत में आरएंडडी और वैरायटी डेवलपमेंट को व्यवस्थित रूप से समर्थन नहीं मिला, तो देश की सभी विद्यमान किसान किस्मों के पंजीकरण के बाद नए पंजीकरण में गिरावट की आशंका है।
दूसरा, सर्टिफिकेट रखने वाले किसानों को राष्ट्रीय कृषि प्रणाली और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों से उनकी स्थानीय फसल किस्मों को मुख्यधारा में लाने के लिए बहुत कम संस्थागत समर्थन मिलता है। केवल आईपी संरक्षण से उनकी किस्में बीज बाजार में उपलब्ध नहीं हो जातीं। इसके लिए उन्हें राज्य की वैरायटी रिलीज कमेटियों में शामिल करना, पैकेजिंग, लेबलिंग और विपणन की व्यवस्था करना आवश्यक है। जैसे-जैसे भारत अपने कृषि-खाद्य तंत्र में पोषण सुरक्षा और जलवायु अनुकूलता हासिल करना चाहता है, किसान किस्मों के लिए समर्थन और अधिक महत्वपूर्ण होता जाएगा।
उधर, औपचारिक बीज उद्योग आईपी-संरक्षित किस्मों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। आईपी समर्थक बीज उद्योग, जिसमें फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया और उनके लाइसेंसी नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया शामिल हैं, कानून में उद्योगों की मदद वाले संशोधनों की लगातार मांग कर रहे हैं, जिनमें ‘वन नेशन वन लाइसेंस’ जैसी नियामक व्यवस्था शामिल है। उनका तर्क है कि इससे कृषि व्यवसाय में सुगमता बढ़ेगी और पीपीवी एंड एफआर अधिनियम, बीज अधिनियम तथा जैव विविधता अधिनियम — इन तीन अलग-अलग कानूनों के कानूनी प्रावधानों का एकीकरण संभव होगा।
आईपी अधिकतावादी (मैक्सिमलिस्ट) शक्तियों के प्रभुत्व के दौर में विशिष्ट रूप से किसान पक्षधर बने रहना ही इस संशोधन प्रक्रिया की वास्तविक परीक्षा होगी।
(शलिनी स्वतंत्र विधि और नीतिगत विश्लेषक हैं। वह 1995 में डब्ल्यूटीओ के अमल में आने के बाद से कृषि में आईपी नियमों पर नजर रख रही हैं)



 Join the RuralVoice whatsapp group
Join the RuralVoice whatsapp group