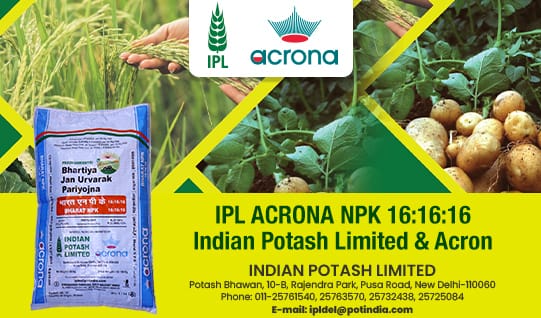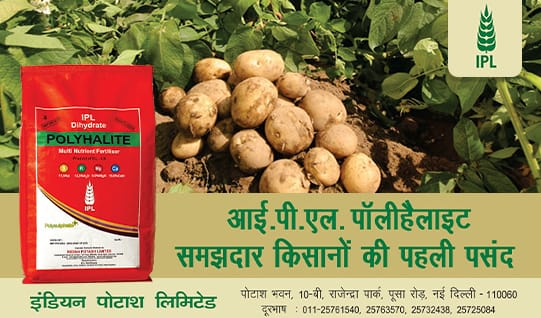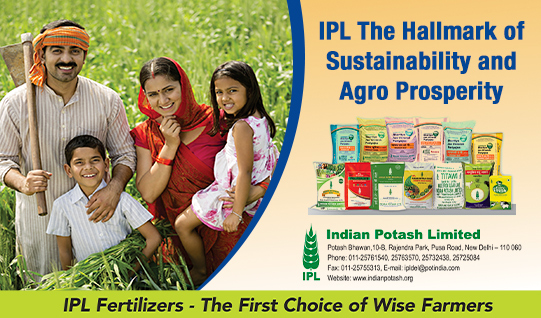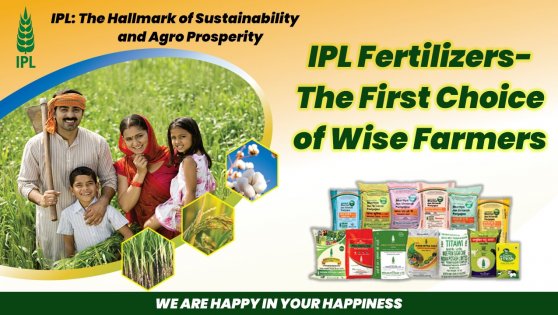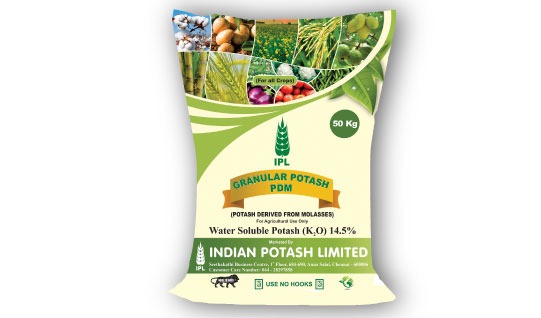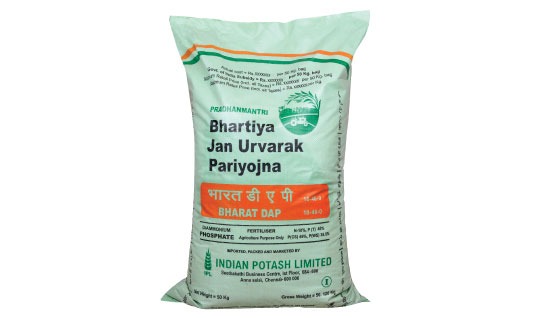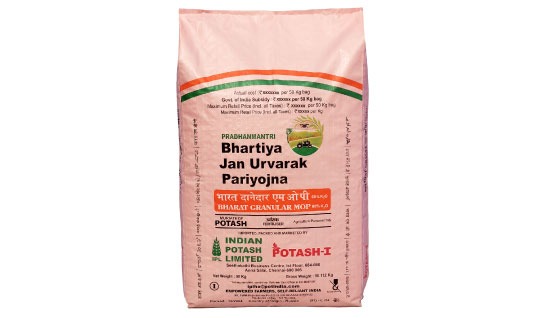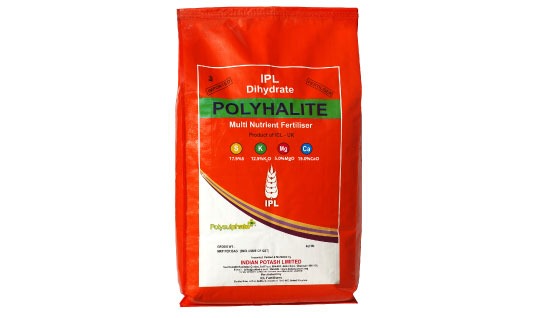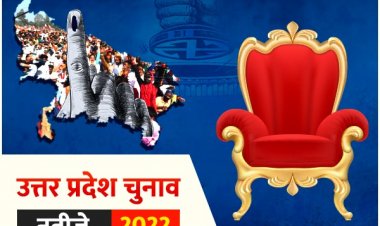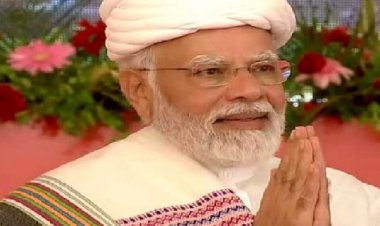धरती का भविष्य हमारी थाली पर निर्भर
आज की दोषपूर्ण खाद्य प्रणाली दुनिया के सबसे बड़े संकटों की वजह बन रही है। एक नई रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि पर्यावरण अनुकूल आहार और कृषि पद्धतियों की ओर बढ़ना अब अनिवार्य हो गया है। मौजूदा तौर-तरीके न केवल धरती को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डाल रहे हैं।

इस मानव युग में, केवल जीवाश्म ईंधन ही हमारे सबसे बड़े वैश्विक संकटों का कारण नहीं हैं, बल्कि भोजन भी इन संकटों—चाहे वह ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन हो, भूमि उपयोग में बदलाव, जैव विविधता का नुकसान या मीठे पानी की कमी—को बढ़ा रहा है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य पोषक तत्वों के अत्यधिक बहाव का सबसे बड़ा स्रोत भी भोजन ही है, जो दुनिया भर में यूट्रोफिकेशन (जलाशयों में पोषक तत्वों की अत्यधिक वृद्धि) को बढ़ावा देता है।
अक्टूबर 2025 की ‘EAT-लैंसेट कमीशन ऑन हेल्दी, सस्टेनेबल एंड जस्ट फूड सिस्टम्स’ रिपोर्ट नए प्रमाण प्रस्तुत करती है कि बढ़ती वैश्विक आबादी का पोषण कैसे किया जाए, जो सभी के लिए न्यायसंगत हो और साथ ही धरती की सीमाओं के भीतर भी रहे। आहार संबंधी निर्णय महत्वपूर्ण हैं क्योंकि बाजार के संकेत (खपत पैटर्न) और सरकारी नीतियों, जैसे पीडीएस के तहत खरीद, के आधार पर किसान तय करते हैं कि क्या उगाएं।
दुर्भाग्य से, आज की दोषपूर्ण खाद्य प्रणाली धरती को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य को भी बिगाड़ रही है। एक-चौथाई से अधिक वैश्विक आबादी या तो कुपोषण का शिकार है या मोटापे से ग्रसित। मौजूदा प्रणाली हर साल लगभग 1.1 करोड़ अकाल मौतों में योगदान देती है और हृदय, श्वास संबंधी और अन्य पुरानी बीमारियों को बढ़ावा दे रही है।
पिछले दशक में, दुनिया ने जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से हटाने और अक्षय ऊर्जा में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया। जबकि जलवायु परिवर्तन में भोजन की भूमिका को नजरअंदाज किया गया। भले ही जीवाश्म ईंधन पर नेट न्यूट्रैलिटी हासिल हो जाए, लेकिन जलवायु चुनौती बनी रहेगी। क्योंकि भोजन एक “लुप्त कड़ी” है और भारत की कृषि उत्पादन एवं उपभोग नीतियां अक्सर इस लक्ष्य के विपरीत काम करती हैं।
पॉट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च द्वारा विकसित EAT-लैंसेट रिपोर्ट पृथ्वी की सहन सीमाओं के भीतर एक स्वस्थ संदर्भ आहार को परिभाषित करती है। प्लैनेटरी हेल्थ डाइट (PHD) की कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:
- सप्ताह में केवल चार बार एनिमल प्रोटीन का सेवन—एक बार चिकन, दो बार मछली, और रोज़ एक बार डेयरी; साथ ही सप्ताह में डेढ़ अंडा
- रेड मीट के उपभोग को लगभग 14 ग्राम प्रतिदिन या सप्ताह में एक बार तक सीमित करना। (यह अमेरिका और यूरोप के औसत से कई गुना कम है। भारत जैसे देशों में आहार धरती की सहन-सीमाओं के भीतर इसलिए रहता है क्योंकि बड़ी आबादी मीट, पॉल्ट्री या अधिक प्रोटीन का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है।)
प्लैनेटरी हेल्थ डाइट (PHD) प्राप्त करने के लिए आयोग के सुझाव:
- कृषि सब्सिडी को मांस और डेयरी की बजाय पर्यावरण-अनुकूल फल-सब्जियों, फलियों और अनाज पर केंद्रित किया जाए। ताकि ये स्वस्थ और टिकाऊ विकल्प और अधिक किफायती बन सकें।
- प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों में कृषि के विस्तार और जैव विविधता के नुकसान को रोका जाए
- भूमि और जल उत्पादकता में सुधार
- कृषि प्राथमिकताओं का पुनर्निर्देशन
- पांच दशकों तक एकल फसल (मोनोकल्चर) उपज में शोध और निवेश को बढ़ावा देने के बाद अब मिश्रित, एकीकृत कृषि प्रणालियों को भी इतना ही महत्व दिया जाए
विश्वविद्यालयों व शोध संस्थानों के सामने चुनौती केवल सतत गहनता के जरिए पर्यावरण अनुकूल और पारंपरिक कृषि का समन्वय करना ही नहीं है, बल्कि इस ज्ञान को विकासशील देशों के साथ मुक्त रूप से साझा करना भी है। जहां उपज उच्चतम स्तर पर है लेकिन कृषि असंतुलित तरीकों से हो रही है, वहां सस्टेनेबिलिटी की ज्यादा जरूरत है जबकि कम पैदावार वाले क्षेत्रों को सतत गहनता पर ध्यान देना चाहिए।
भारत का फोकस शोध के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने के बजाय खरीद-प्रोत्साहन के जरिए उत्पादन बढ़ाने पर रहा है। पेरिस समझौते के लक्ष्य हासिल करने का एकमात्र तरीका है वैश्विक खाद्य प्रणाली में परिवर्तन यानी आहार में बदलाव, कार्बन उत्सर्जन और खाद्य अपशिष्ट को आधा करना, तथा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अपनाना। इसमें नाइट्रोजन व फास्फोरस के बहाव को कम करना, उर्वरकों और गोबर से नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन घटाना और पशुधन से मीथेन उत्सर्जन कम करना शामिल है। लेकिन भारत इन मोर्चों पर पिछड़ रहा है। रसायनों पर बढ़ती निर्भरता संकट को और गहरा कर रही है।
प्लैनेटरी हेल्थ डाइट के मूल में न्याय का सिद्धांत है। इसके अनुसार किसान सिर्फ खाद्य उत्पादक नहीं हैं, वे सम्मानजनक आजीविका के हकदार भी हैं। फिर बड़ा सवाल यह है कि किसान पर्यावरण-अनुकूल कृषि पद्धतियां कैसे अपनाएं, जबकि भोजन को सस्ता रखने पर आधारित लोकलुभावन राजनीति कृषि उपज के दाम बढ़ने से रोकती है?
यदि डोनाल्ड ट्रम्प सब्सिडी वाला अमेरिकी अनाज खरीदने के लिए दबाव बनाते हैं, तो भारत जैसे खाद्य-आयातक देशों में कृषि उपजों के मूल्य और गिरेंगे। इससे किसान और गरीबी में धकेले जाएंगे, और असंतुलित एकल-कृषि का चक्र चलता रहेगा।
जलवायु परिवर्तन को राजनीतिक सीमाओं के भीतर सीमित रखकर हल नहीं किया जा सकता। दुनिया को यह पुनर्विचार करना होगा कि कृषि उपज का व्यापार किस तरह किया जाए — खासकर विश्व व्यापार संगठन (WTO) के ढांचे के भीतर — और उसकी असल लागत उपभोक्ता की थाली में किस रूप में दिखाई दे।
(अजय वीर जाखड़ भारत कृषक समाज के चेयरमैन हैं)



 Join the RuralVoice whatsapp group
Join the RuralVoice whatsapp group