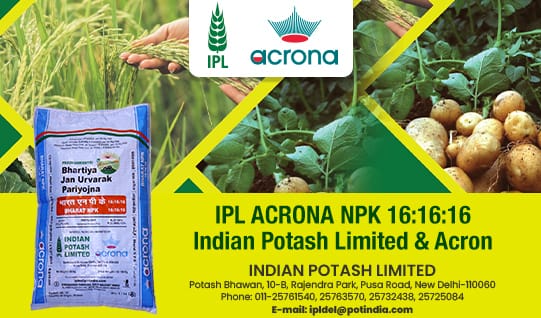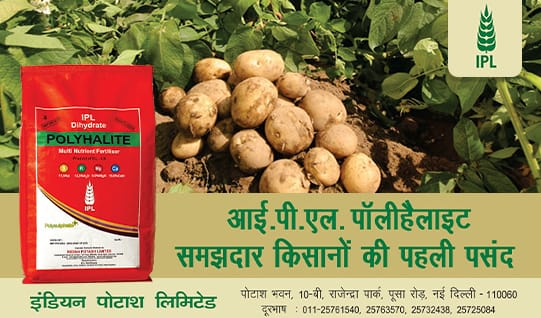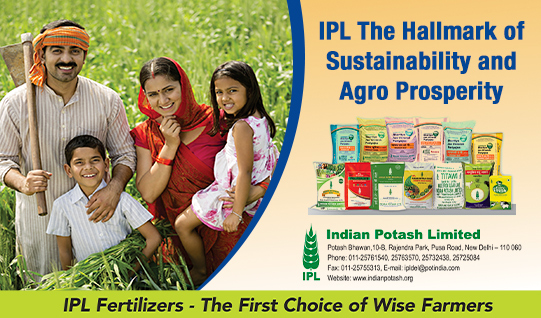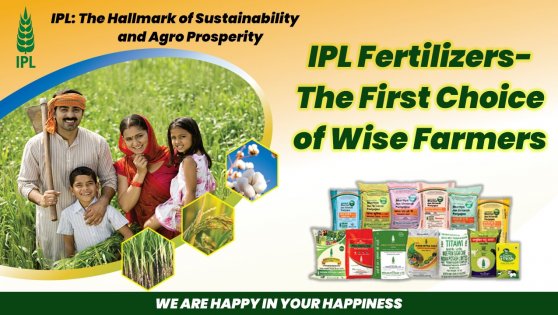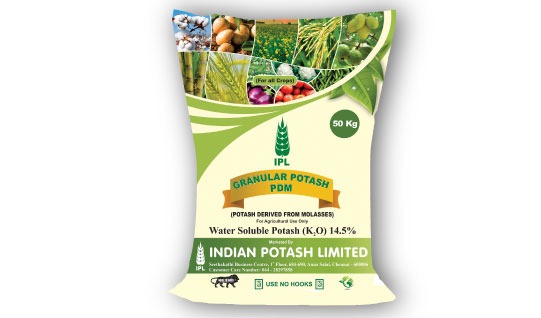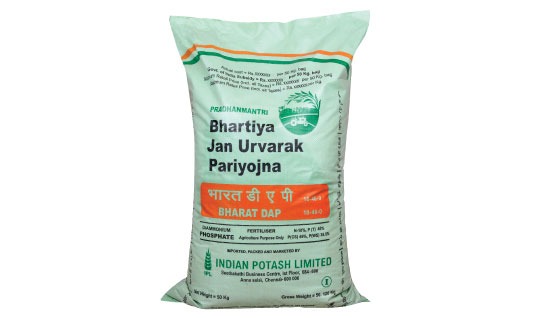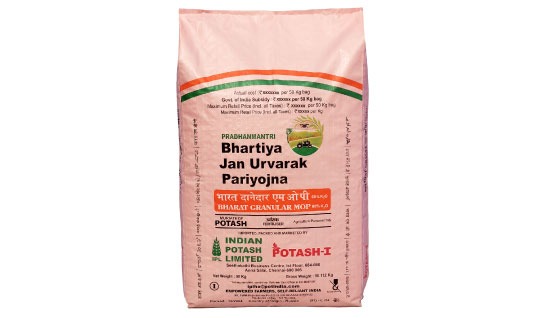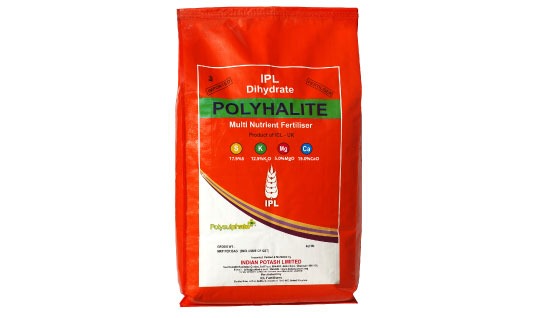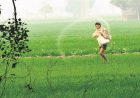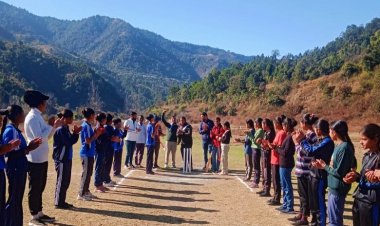बायो एनर्जी से नेट-जीरो लक्ष्य की प्राप्ति - जैव ऊर्जा में भारत की अब तक की नीतिगत पहल और भविष्य के मार्ग
भारत की बायोएनर्जी यात्रा 1980 के दशक में गोबर गैस संयंत्रों से शुरू होकर एथेनॉल ब्लेंडिंग, बायोडीजल, सीबीजी प्लांट और बिजली उत्पादन में बायोमास उपयोग तक पहुंची है। 2018 की राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति और SATAT योजना ने इसे गति दी, हालांकि चुनौतियां बनी हुई हैं। कार्बन फंड और नीतिगत स्थिरता बायोएनर्जी ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय और नेट-जीरो लक्ष्यों को मजबूत करेगी।

भारत का जैव ऊर्जा (बायो एनर्जी) से जुड़ाव 1980 के दशक में शुरू हुआ। तब कृषि अपशिष्ट, विशेषकर मवेशियों के गोबर, को ग्रामीण घरों के लिए स्वच्छ रसोई गैस में बदलने का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया गया था। हालांकि उस समय पर्यावरण संबंधी चिंताएं मुख्य प्रेरक नहीं थीं, फिर भी यह पहल समय के लिहाज से दूरदर्शी थी। इसका उद्देश्य किसानों को खाना पकाने और रौशनी के लिए आधुनिक, धुआं-मुक्त ऊर्जा विकल्प प्रदान करना था। भारत सरकार ने स्वच्छ और स्वस्थ जीवनशैली प्रदान करने के उद्देश्य से ऐसी इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की।
इस दिशा में अगली बड़ी छलांग 2003 में लगी जब इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। चुनिंदा राज्यों में पेट्रोल में 5% तक इथेनॉल मिश्रण अनिवार्य कर दिया गया। इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा पैदा करने के साथ जीवाश्म ईंधन का आयात कम करना था। इसी के साथ जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता से नवीकरणीय ऊर्जा में आत्मनिर्भरता की दिशा में बदलाव की भी शुरुआत हुई। प्रारंभ में गन्ने के सह-उत्पाद, जैसे मोलेसेज का उपयोग इथेनॉल उत्पादन के लिए किया जाता था। वर्ष 2005 में भारत ने बायोडीजल खरीद नीति के साथ अपनी जैव ऊर्जा दृष्टि का विस्तार किया, और 2012 तक डीजल के साथ बायोडीजल के मिश्रण को 20% तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया। योजना आयोग ने इसके लिए जिस मुख्य फीडस्टॉक पर भरोसा किया था, वह था अखाद्य तिलहन और जट्रोफा।
लगभग उसी समय चीनी मिलों, चावल मिलों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में को-जनरेशन प्लांट फलने-फूलने लगे, जिससे लागत में बचत हुई, उत्सर्जन में कमी आई और जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी आई। सरकार ने इन संयंत्रों की स्थापना में वित्तीय सहायता दी।
शुरुआती प्रगति धीमी
इन प्रयासों के बावजूद इथेनॉल और बायोडीजल मिश्रण में शुरुआती प्रगति धीमी रही। वर्ष 2014 तक इथेनॉल मिश्रण 1.5% से कम रहा और डीजल के मामले में तो यह और भी कम था। इसका मुख्य कारण खंडित नीतियां और वैश्विक परिवेश था जहां जीवाश्म ईंधन का आयात आसान लगता था। लेकिन तेल की बढ़ती कीमतों और ऊर्जा सुरक्षा की रणनीतिक जरूरत ने बदलाव की मांग की। यह बदलाव 2014 में आया जब पेट्रोल की कीमत 31 रुपये से बढ़कर 81 रुपये हो गई, जो एक दशक में ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा वृद्धि थी।
एक मजबूत ऊर्जा रणनीति की तात्कालिकता को समझते हुए एनडीए सरकार ने जैव ईंधन क्षेत्र को पुनर्जीवित किया, जिसके परिणामस्वरूप 2018 में क्रांतिकारी राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति लागू हुई। इस ऐतिहासिक नीति ने इथेनॉल के लिए फीडस्टॉक आधार का विस्तार किया और इसमें चीनी सिरप, मक्का, खराब खाद्यान्न और यहां तक कि बायोडीजल के लिए प्रयुक्त खाद्य तेल को भी शामिल किया। इसने 2जी इथेनॉल जैसे उन्नत जैव ईंधनों में निवेश को भी प्रोत्साहित किया और एक आकर्षक मूल्य निर्धारण प्रणाली की शुरुआत की। इससे इथेनॉल उत्पादन व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य हो गया। पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य मूल रूप से 2030 के लिए निर्धारित था, लेकिन महत्वाकांक्षी रूप से पीछे करते हुए 2025-26 तक कर दिया गया।
उसी वर्ष भारत ने सस्ते परिवहन के लिए सतत विकल्प (SATAT) योजना शुरू की। यह कृषि अवशेषों, नगरपालिका अपशिष्ट और बायोमास से कंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) बनाने वाले 5,000 संयंत्र स्थापित करने की एक दूरदर्शी योजना थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल कच्चे तेल के आयात में कटौती करना था, बल्कि एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना भी जहां अपशिष्ट को धन में परिवर्तित किया जा सके, ताकि किसानों को आय का एक अतिरिक्त स्रोत मिले और परिवहन के लिए स्वच्छ ईंधन भी सुनिश्चित हो।
इथेनॉल मिश्रण में प्रगति
इथेनॉल मिश्रण में प्रगति उत्साहजनक रही और पिछले एक दशक में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। हालांकि बायोडीजल अब भी कच्चे माल की कमी के कारण चुनौतियों का सामना कर रहा है। जिस जट्रोफा फसल पर सरकार ने शुरुआत में भरोसा किया था, वह सफल नहीं हुई। शायद प्रयोगशाला में उगाई गई और खेतों में उगाई गई फसलों में बहुत अंतर था, जिसके कारण यील्ड और एफिशिएंसी बुरी तरह प्रभावित हुई। एग्रीगेशन संबंधी समस्याओं और मिलावट के बाजार में भेजे जाने के कारण प्रयुक्त खाद्य तेल का संग्रह भी ठीक से काम नहीं कर पाया। उद्योग ने एक और कच्चा माल, पाम तेल आजमाया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव, आयात पर निर्भरता और कम उठाव मूल्य के कारण यह भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका।
2018 से 2023 तक सीबीजी की ग्रोथ भी बहुत धीमी रही। उस दौरान 40 से 50 संयंत्र ही स्थापित किए जा सके। इस पर ध्यान देते हुए केंद्र सरकार ने कुछ नीतिगत उपाय किए, जिनमें फर्मेंटेड जैविक खाद (एफओएम) के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए), बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी (बीएएम) योजना, प्रत्यक्ष पाइपलाइन इंजेक्शन (डीपीआई) योजना, केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) आदि शामिल हैं। इनसे उद्योग को थोड़ा बढ़ावा मिला। अब देश में लगभग 120 संयंत्र चालू हो चुके तथा 200 से 300 अन्य निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।
एक और आशाजनक प्रगति बॉयलरों में सघन बायोमास का उपयोग है, विशेष रूप से बिजली के क्षेत्र में। ऊर्जा मंत्रालय ने ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के साथ 5% बायोमास मिश्रण का लक्ष्य रखा है। थर्मल प्लांट में कृषि-अवशेषों के उपयोग पर सतत कृषि मिशन को सुगम बनाने के लिए समर्थ मिशन की स्थापना की गई ताकि एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा सके जो उठाव में सहायक हो। मूल्य बेंचमार्किंग भी शुरू की गई और इससे इस क्षेत्र में आवश्यक सकारात्मक गति लाने में मदद मिली।
भविष्य की तैयारियां
आगे की बात करें तो भारत 2जी इथेनॉल, सतत विमान ईंधन (एसएएफ) और जैव-सामग्री जैसे भविष्योन्मुखी क्षेत्रों में भी निवेश कर रहा है। ये भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत ने 2030 तक कार्बन तीव्रता में 45% की कमी, 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता और 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है।
सरकार का इरादा स्पष्ट है, लेकिन इस सेक्टर की पूरी क्षमता को हासिल करने के लिए मदद बढ़ाना और एक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र बनाना आवश्यक है। खंडित प्रयासों के बजाय एक व्यापक, सतत दृष्टिकोण ही आगे बढ़ने का रास्ता होगा। इसके प्रमुख कारक होंगे:
- एक प्राइस गैप सपोर्ट तंत्र, जो ईंधन को किफायती रखते हुए उत्पादकों के लिए उचित लाभ सुनिश्चित करे।
- बायो एनर्जी के वित्तपोषण के लिए जीवाश्म ईंधन उपकर पर आधारित एक केंद्रीय जलवायु और कार्बन रिडक्शन फंड।
- दीर्घकालिक निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए मैंडेट और नीतिगत निश्चितता।
भारत की जैव ऊर्जा यात्रा अब केवल तेल आयात कम करने तक सीमित नहीं है। यह किसानों को सशक्त बनाने, अपशिष्ट प्रबंधन को स्थायी बनाने, हरित रोजगार सृजन और भारत को रिन्यूएबल एनर्जी इनोवेशन में दुनिया में अग्रणी के रूप में स्थापित करने के बारे में है। निर्णायक नीतियों, उद्योगों के सहयोग और मजबूत जन समर्थन के साथ जैव ऊर्जा भारत के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की आधारशिला बन सकती है।
(लेखक इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी के डायरेक्टर जनरल हैं। यहां व्यक्त विचार निजी हैं)



 Join the RuralVoice whatsapp group
Join the RuralVoice whatsapp group