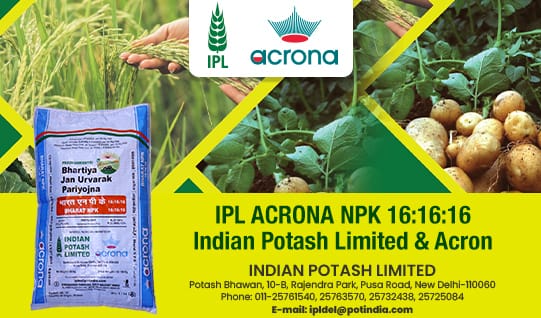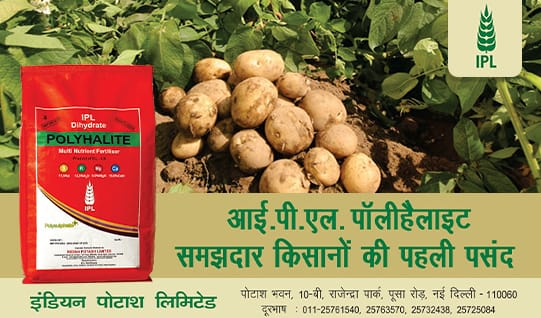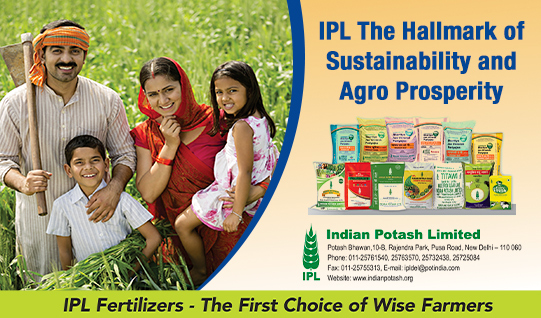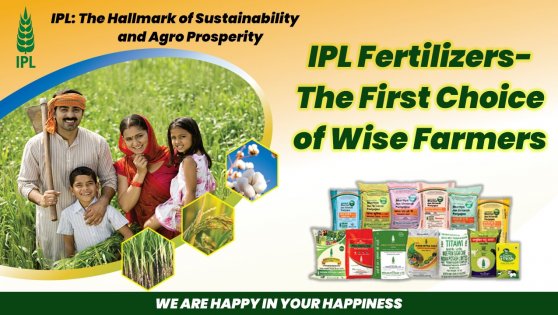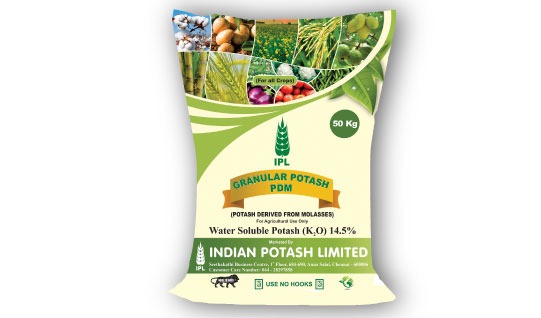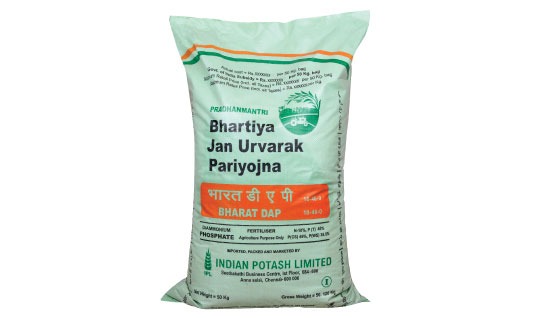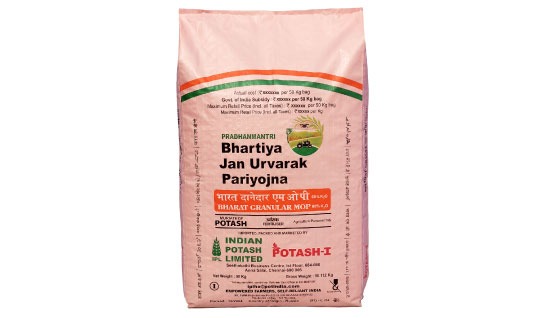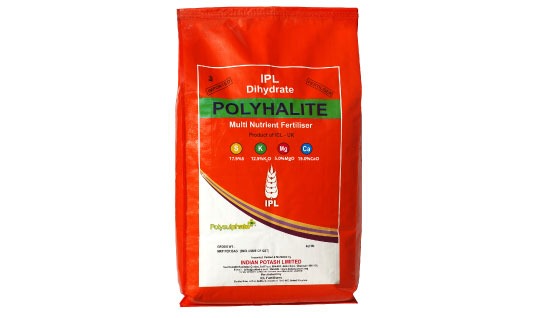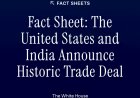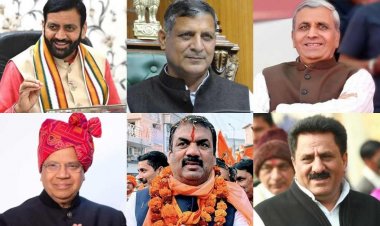फसलों में पोषणः पोषक तत्व आपूर्ति के स्थायी स्रोत बन सकते हैं जैव उर्वरक
दशकों के शोध से पता चलता है कि जैव उर्वरक स्थायी रूप से एक-चौथाई रासायनिक पोषक तत्वों की जगह ले सकते हैं। इनके प्रयोग से न सिर्फ पैदावार बढ़ेगी बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। आईएआरआई तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के शोध से तैयार जैव उर्वरक सहजता से उपलब्ध भी हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) नई दिल्ली के माइक्रोबायोलॉजी डिवीजन, अन्य आईसीएआर संस्थानों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में जैव उर्वरकों (बायो फर्टिलाइजर) पर दशकों के शोध ने यह सिद्ध कर दिया है कि जैव उर्वरक फसलों के लिए नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P) और पोटाश (K) जैसे प्रमुख पोषक तत्वों की अनुशंसित मात्रा का 25% आसानी से स्थिर (फिक्स) या गतिशील कर सकते हैं। विभिन्न संस्थानों की तरफ से विकसित ऐसे प्रोडक्ट उत्पादन बढ़ाने के लिए सहज उपलब्ध हैं।
पोषक तत्वों की आपूर्ति में जैव उर्वरकों की क्षमता: सभी जैव उर्वरक प्रति हेक्टेयर 20-30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रदान कर सकते हैं, उपज में 12-20% की वृद्धि कर सकते हैं और मिट्टी की उर्वरता में उल्लेखनीय सुधार कर सकते हैं। विशेष रूप से पूसा माइकोराइजा, 30-35% फास्फोरस की पूर्ति करके एक स्थायी समाधान प्रदान करता है। इससे रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है और नर्सरी में उगाई जाने वाली फसलों से लेकर विविध फसलों तक, पर्यावरण-अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिलता है। इन जैव उर्वरकों के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की खपत में अनुमानित 10-25% की कमी संभव है, जिससे किसानों की लागत में उल्लेखनीय बचत होगी।
क्या किया जाना चाहिए?
1. जैव उर्वरकों को प्राकृतिक/जैविक खेती का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए: प्राकृतिक/जैविक खेती में पोषक तत्वों की आपूर्ति बीजामृत, जीवामृत, घनजीवामृत आदि के रूप में सूक्ष्मजीवों की शक्ति का दोहन करने की धारणा पर आधारित है। हालांकि इनमें से कोई भी उत्पाद वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है। इसके विपरीत, विभिन्न संस्थानों द्वारा विकसित जैव उर्वरक दशकों के शोध पर आधारित हैं और प्रकृति में उपलब्ध मिट्टी, गोबर और मूत्र आदि स्रोतों से प्राप्त सर्वाधिक प्रभावी सूक्ष्मजीवों का उपयोग करते हैं। इसलिए जैविक/प्राकृतिक खेती में इन जैव उर्वरकों का उपयोग कहीं अधिक प्रभावी होगा।
2. जैव उर्वरकों को अकार्बनिक कृषि प्रणाली का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए: जैव उर्वरक पोषक तत्वों की 25% पूर्ति करने में सक्षम हैं, इसलिए उन्हें अकार्बनिक कृषि प्रणाली का भी अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। अनुशंसाओं के बावजूद जैव उर्वरकों का व्यवहार में बड़े पैमाने पर उपयोग नहीं हुआ है।

विभिन्न आईसीएआर संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में शोध से तैयार कई जैव उर्वरक उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ का विवरण नीचे दिया गया है।
पूसा जैव उर्वरक
आईसीएआर-आईएआरआई, नई दिल्ली के माइक्रोबायोलॉजी डिवीजन का 1980 के दशक के आरंभ से जैव उर्वरक अनुसंधान एवं विकास में लंबा और विशिष्ट इतिहास रहा है। इस विभाग ने ठोस वाहक आधारित, सिंगल बैक्टीरियल इनोकुलेंट सहित जैव उर्वरकों की एक विस्तृत श्रृंखला के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। इनमें दालों के लिए राइजोबियम, सब्जियों और अनाज के लिए एजोटोबैक्टर, अनाज और बाजरा के लिए एजोस्पिरिलम जैसे शुरुआती इनोवेशन शामिल हैं। इस विभाग ने धान की खेती के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए साइनोबैक्टीरिया-आधारित जैव उर्वरक भी विकसित किए हैं।
पिछले कुछ वर्षों में इस विभाग ने विविध फसलों के लिए उपयुक्त बहु-सूक्ष्मजीव/बहु-पोषक, मल्टी-फंक्शनल, करियर-आधारित और तरल फॉर्मूलेशन तैयार करके उल्लेखनीय प्रगति की है। ये न केवल पौधों/उपज को मजबूत बनाते हैं, बल्कि स्थूल एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता भी बढ़ाते हैं। साथ ही, पौधों की वृद्धि और उपज को उल्लेखनीय रूप से प्रोत्साहित करते हैं। इसके प्रमुख उदाहरणों में बहु-पोषक तत्व प्रदान करने वाले उत्पाद शामिल हैं, जैसे:
1. पूसा सम्पूर्ण: एनपीके (नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम) प्रदान करने वाले लाभकारी सूक्ष्मजीवों का एक कंसोर्टियम।
2. पूसा बायोफर्ट: देसी बैक्टीरिया का एक कंसोर्टियम, साथ ही एजोस्पिरिलम, एजोटोबैक्टर के नए फॉर्मूलेशन और फास्फोरस, पोटेशियम तथा जिंक जैसे आवश्यक पोषक तत्वों को घुलनशील बनाने वाले फॉर्मूलेशन।
3. पूसा माइकोराइजा: पोषक तत्वों और पानी का अवशोषण बढ़ाने, मिट्टी की संरचना में सुधार करने और रोगों तथा पर्यावरणीय दिक्कतों के प्रति पौधों का लचीलापन बढ़ाने के लिए एक माइकोराइजल जैव उर्वरक।
4. पूसा साइनोन्यूट्रिकॉन, पूसा साइनोफोर्ट, पूसा साइनोबायोकॉन: फलियां, सब्जियां, कपास, गेहूं, मक्का जैसी विभिन्न फसलों में उपयोग के लिए नए मल्टी-फंक्शनल, साइनोबैक्टीरियल फॉर्मूलेशन भी विकसित किए गए हैं और विविध कृषि-पारिस्थितिकी में परीक्षण किया गया है। ये ऑर्गेनिक कार्बन में सुधार करते हैं, मिट्टी में नाइट्रोजन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता तथा पौधों में उनका स्थानांतरण बेहतर बनाते हैं, साथ ही प्रति हेक्टेयर 25-30 किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत भी करते हैं।
तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय ने भी ऐसे कई उत्पाद तैयार किए हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है।
इसी प्रकार अन्य आईसीएआर संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के पास दशकों के अनुसंधान से विकसित जैव उर्वरकों की एक श्रृंखला है, जिनका उत्पादन संबंधित संस्थानों द्वारा छोटे पैमाने पर किया जा रहा है। इनमें से कुछ के उत्पादन के लिए छोटी कंपनियों को लाइसेंस भी दिया गया है।
बाधाएं: उचित मूल्य पर और आवश्यक मात्रा में गुणवत्तापूर्ण जैव उर्वरकों की अनुपलब्धता उनके उपयोग की प्रमुख बाधाएं हैं। इसका कारण यह है कि जैव उर्वरकों का उत्पादन और इनकी आपूर्ति मोटे तौर पर अवांछित लोगों के हाथों में रही है। उनके पास शोध आधारित जैव उर्वरकों की उत्पादन सुविधा नहीं है, उत्पादन, भंडारण और परिवहन की स्थिति और आपूर्ति श्रृंखला अच्छी तरह से विकसित नहीं है। अक्सर जैव उर्वरकों को बिना किसी गुणवत्ता नियंत्रण के सब्सिडी के तहत खरीदा जाता है और फिर इनकी आपूर्ति की जाती है। कई बार तो पैकेट में केवल राख (करियर) होती है जिसमें जीवित सूक्ष्मजीव नहीं होते। यह जैव उर्वरकों के प्रभावी न होने के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक रहा है।
क्या किया जाना चाहिए: सख्त गुणवत्ता नियंत्रण वाली छोटी कंपनियों के अलावा, एक समग्र आपूर्ति श्रृंखला के साथ जैव उर्वरकों के उत्पादन की प्रमुख जिम्मेदारी इफको, कृभको, एनएफएल, नागार्जुन फर्टिलाइजर्स जैसी प्रमुख उर्वरक कंपनियों को दी जानी चाहिए। यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि ये कंपनियां अपने कुल पोषक उत्पादन का 25% जैव उर्वरकों के रूप में उत्पादित करें। उन्हें इसके लिए अपने सीएसआर फंड का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है।
प्रभाव: जैव उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 25% की कमी आएगी और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन भी इसी अनुपात में कम होगा। भारत में कृषि से कुल नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन 3 लाख टन है, जिसमें से 20% सिंथेटिक उर्वरकों से होता है। जैव उर्वरकों के उपयोग से उत्सर्जन में 20% के 25% यानी 15,000 टन नाइट्रोजन ऑक्साइड की कमी आएगी, साथ ही किसानों की खेती की लागत भी कम होगी। जैव उर्वरकों के प्रति किसानों का विश्वास बढ़ाने के लिए उनके खेतों पर इन उत्पादों का बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी आवश्यक है।
(लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक हैं। लेख में व्यक्त विचार उनके निजी हैं)



 Join the RuralVoice whatsapp group
Join the RuralVoice whatsapp group